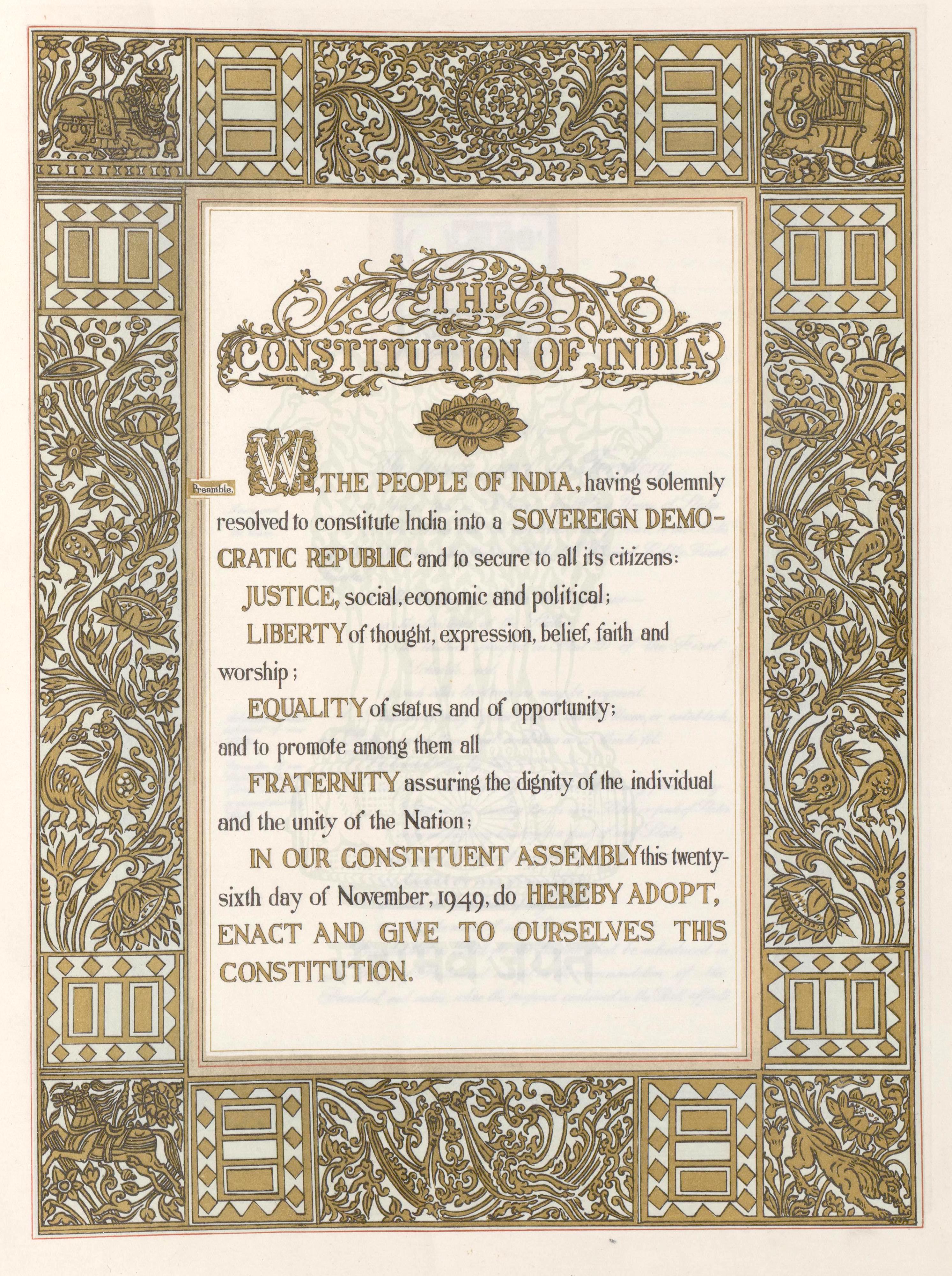ज्योति बसु और संसदीय वामपन्थी राजनीति की आधी सदी
ज्योति बसु (1914-2010) के निधन के अवसर पर
ज्योति बसु नहीं रहे। विगत 17 जनवरी 2010 को 96 वर्ष का लम्बा जीवन जीने के बाद कलकत्ता के एक अस्पताल में उन्होंने अन्तिम साँस ली। निधन के दिन से लेकर अन्तिम यात्रा (उन्होंने अपना शरीर मेडिकल रिसर्च के लिए दान कर दिया था) तक बुर्जुआ राजनीतिक हलकों में उन्हें उसी सम्मान के साथ याद किया गया और श्रद्धांजलि दी गयी, जितना सम्मान आज़ादी के बाद देश के शीर्षस्थ बुर्जुआ नेताओं को दिया जाता रहा है।
माकपा, भाकपा, आर.एस.पी., फ़ॉरवर्ड ब्लॉक आदि रंग-बिरंगी चुनावी वामपन्थी पार्टियों के नेताओं के अतिरिक्त प्रधानमन्त्री और सोनिया गाँधी से लेकर सभी बुर्जुआ दलों के नेताओं ने कलकत्ता पहुँचकर ज्योति बसु को श्रद्धांजलि दी। कई पूँजीपतियों ने बंगाल में पूँजी लगाने में उनके सहयोग को भावविह्नल होकर याद किया। टाटा, बिड़ला, जैन आदि सभी छोटे-बड़े पूँजीपति घरानों के छोटे-बड़े अंग्रेज़ी-हिन्दी अख़बारों ने उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए स्मृति लेख लिखे। कुछ टुटपूँजिया टिप्पणीकारों ने आश्चर्य प्रकट किया कि इतना भलेमानस आदमी कम्युनिस्ट क्यों और कैसे था? किसी ने लिखा कि वे भले आदमी पहले थे और कम्युनिस्ट बाद में। समझदार बुर्जुआ टिप्पणीकारों ने ऐसी बातें नहीं की। वे जानते हैं कि ज्योति बसु जैसे संसदीय कम्युनिस्टों की इस व्यवस्था को कितनी ज़रूरत होती है! यदि उनके ऊपर ''कम्युनिस्ट'' का लेबल ही नहीं रहेगा, तो वे पूँजीवादी व्यवस्था के लिए उतने उपयोगी भी नहीं रहे जायेंगे।
ज्योति बसु एक 'भद्रलोक' (जेण्टलमैन) कम्युनिस्ट थे शालीन, नफ़ीस, सुसंस्कृत। वे क्रान्ति और संघर्ष की वे बातें नहीं करते थे, जो खाते-पीते फ्जेण्टलमैन'' सुधारवादी मधयवर्ग को भाती नहीं। ज्योति बसु की जीवन-शैली, कार्य-शैली उनकी राजनीति के सर्वथा अनुरूप थी। इसलिए फ्सामाजिक अशान्ति'' से भयाकुल रहने वाले मधयवर्ग के उन लोगों को और (आदतों एवं जीवनशैली में मधयवर्ग बन चुके) सपफेदपोश कुलीन मज़दूरों को वे काफ़ी भाते थे। जो दयालु, करुणामय और फ्शान्तिप्रिय'' मधयवर्गीय भलेमानस पूँजीवादी व्यवस्था को आमूल रूप से बदल डालने के फ्ख़तरनाक और जोखिम भरे झंझट'' से दूर रहकर इसी व्यवस्था को सुधारकर ग़रीब-ग़ुरबा की ज़िन्दगी में भी बेहतरी लाने के भ्रम में जीते हैं और ऐसा भ्रम पैदा करते हैं, जो लोग पूँजीवादी उत्पादन-प्रणाली के क्षुद्र रहस्य और पूँजीवादी राजनीतिक तन्त्र के अपरिवर्तनीय वर्ग-चरित्रा को समझे बिना यह सोचते रहते हैं कि यदि नेता भ्रष्टाचारी न हों और नौकरशाही- लालफ़ीताशाही न हो तो सबकुछ ठीक हो जायेगा, ऐसे भोले-भाले, नेकनीयत मधयवर्ग के लोगों को भी ज्योति बसु, नम्बूदिरिपाद, सुन्दरैया जैसे व्यक्तित्व बहुत भाते हैं। यह भी सामाजिक जनवाद या संशोधनवादी राजनीति की एक सफ़लता है।
ज्योति बसु सादगी भरा, लेकिन उच्च मधयवर्गीय कुलीन जीवन जीते थे, लेकिन उनपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया जा सकता। उनसे भी अधिक सादा जीवन माकपा के गोपालन, सुन्दरैया, नम्बूदिरिपाद, हरेकृष्ण कोन्नार, प्रमोद दासगुप्ता जैसे नेताओं का था। पर बुनियादी सवाल किसी नेता के सादगी और ईमानदारी भरे निजी जीवन का नहीं है। बुनियादी सवाल यह भी नहीं है कि वह नेता समाजवाद और कम्युनिज्म की बातें करता है। बुनियादी सवाल यह है कि क्या समाजवाद और कम्युनिज्म की उसकी बातों का वैज्ञानिक आधार है, क्या उसकी नीतियाँ एवं व्यवहार अमली तौर पर मज़दूर वर्ग को उसकी मुक्ति की निर्णायक लड़ाई की दिशा में आगे बढ़ाते हैं? सादा जीवन गाँधी का भी था और अपने बुर्जुआ मानवतावादी सिद्धान्तों पर उनकी निजी निष्ठा पर भी सन्देह नहीं किया जा सकता। उनके मानवतावादी यूटोपिया ने करोड़ों आम जनों को जागृत-सक्रिय किया, लेकिन उस यूटोपिया को अमल में लाने की हर प्रकार की कोशिश की अन्तिम परिणति पूँजीवादी सामाजिक-आर्थिक ढाँचे की स्थापना के रूप में ही सामने आनी थी। कहने का मतलब यह कि बुनियादी प्रश्न किसी के ईमानदार नैतिक जीवन और उसकी यूटोपियाई निजी निष्ठाओं का नहीं, बल्कि उसकी विचारधारात्मक-राजनीतिक वर्ग- अवस्थिति का होता है। एक सच्चा और ईमानदार व्यक्ति यदि बुर्जुआ राजनीति के दायरे में ही काम करता है, तो वह वस्तुगत रूप से बुर्जुआ वर्ग की ही सेवा करेगा और उसकी अच्छी छवि बुर्जुआ व्यवस्था के प्रति लोगों का विभ्रम मज़बूत बनाने में मददगार ही बनेगी। लेकिन चूँकि हमारे सामाजिक व्यवहार से ही हमारी चेतना निर्मित-अनुकूलित होती है, इसलिए एक ग़लत राजनीति को वस्तुगत तौर पर लागू करने वाले लोग कालान्तर में सचेतन तौर पर भी ग़लत हो जाते हैं और निजी जीवन के स्तर पर भी ढोंग-पाखण्ड, झूठ-फ़रेब और भ्रष्टाचार से लबरेज़ हो जाते हैं। संशोधनवादी पार्टियों के बहुतेरे पुराने नेता व्यक्तिगत तौर पर भ्रष्ट-पतित नहीं, बल्कि भद्र नागरिक थे। आज यह बात नहीं कही जा सकती। इन पार्टियों में ऊपर यदि भ्रष्ट-पतित लोगों की भरमार है, तो नीचे क़तारों में गली के गुण्डे-लपफंगे तक घुस गये हैं। इनका यह सामाजिक चारित्रिाक पतन सामाजिक जनवाद/ संशोधनवाद/संसदीय वामपन्थ के क्रमिक राजनीतिक पतन-विघटन की ही एक परिणति है, एक अभिव्यक्ति है और एक प्रतिबिम्ब है। सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के देशों में नकली समाजवाद का झण्डा (ख्रुश्चेव काल से सोवियत संघ ही संशोधनवादियों का मक्का था) 1990 में गिर गया। फ़िर चीन में 1976 में माओ की मृत्यु के बाद देघपन्थी संशोधनवाद की जो सत्ता क़ायम हुई थी, उसका फ्बाज़ार समाजवाद'' अब सरेबाज़ार अलफ़ नंगा खड़ा अपनी पूँजीवादी असलियत की नुमाइश कर रहा है। ऐसी सूरत में, दुनिया भर की रंग-बिरंगी ख्रुश्चेवी संशोधनवादी पार्टियों ने ज्यादा खुले तौर पर पूँजीवादी संसदीय राजनीति और अर्थवादी राजनीति की चौहद्दी को स्वीकार कर लिया है। अब उनका बात-व्यवहार एकदम खुले तौर पर (सारतत्व तो पहले से ही एक था) वैसा ही हो गया है जैसा कि 1910 के दशक में मार्क्सवाद से विपथगमन करने वाली काउत्सकीपन्थी सामाजिक जनवादी पार्टियों का रहा है। यूरोप से लेकर कई लातिन अमेरिकी देशों तक में लेबर पार्टियों और सोशलिस्ट पार्टियों का आचरण दक्षिणपन्थी बुर्जुआ पार्टियों जैसा हो गया है तथा ख्रुश्चेवी कम्युनिस्ट पार्टियों का आचरण लेबर और सोशलिस्ट पार्टियों जैसा हो गया है। भारत में कुछ पुराने समाजवादी फ़ासिस्ट भाजपा के साथ गाँठ जोड़ सरकारें चला रहे हैं, कुछ धानी किसानों-कुलकों की राजनीति कर रहे हैं तो कुछ अलग-अलग बुर्जुआ पार्टियों में घुल-मिल गये हैं। जो ख्रुश्चेवी और देंगपन्थी संशोधनवादी पार्टियाँ हैं, वे भूमण्डलीकरण की पूरी राजनीति एवं अर्थनीति को स्वीकारते हुए बस उसे कुछ फ्मानवीय चेहरा'' देने की बात करती हैं तथा सरपट उदारीकरण- निजीकरण की राह में कुछ स्पीड-ब्रेकर्स लगाने की बात करती हैं, ताकि मेहनतकश अवाम का पूँजीवादी व्यवस्था और संसदीय राजनीति के प्रति भरम बने रहे तथा निर्बाधा उदारीकरण- निजीकरण की भयंकर सामाजिक परिणतियाँ (बेशुमार छँटनी, बेरोज़गारी, विस्थापन, मज़दूरों के रहे-सहे अधिकारों एवं सामाजिक सुरक्षा का भी अपहरण, धानी-ग़रीब की बढ़ती खाई आदि) किसी क्रान्तिकारी तूफ़ान के उभार के लिए ज़रूरी सामाजिक दबाव न पैदा कर दें। इस तरह, अपनी छद्म वामपन्थी जुमलेबाज़ी को छोड़ देने और बुर्जुआ चेहरे से नक़ाब थोड़ा हटा देने के बावजूद, पूरी दुनिया की ही तरह, भारत की संशोधनवादी वामपन्थी पार्टियाँ अभी भी इस व्यवस्था की वफ़ादार सुरक्षा पंक्ति की, सामाजिक ताप पर ठण्डा पानी डालते रहने वाले पुफहारे की तथा जनाक्रोश के दाब को कम करने वाले सेफ़्रटीवॉल्व की भूमिका अत्यन्त कुशलतापूर्वक निभा रही हैं। उनके फ्कम्युनिज्म'' को लेकर जनता को कोई भ्रम नहीं रह गया है और इस मायने में उनकी एक भूमिका (भ्रमोत्पादक की भूमिका) तो समाप्त हो चुकी है, लेकिन फ्वाम'' सुधारवादी राजनीतिक शक्ति के रूप में पूँजीवाद की दूसरी सुरक्षा-पंक्ति के रूप में उनकी भूमिका अभी भी क़ायम है। नवउदारवाद की राजनीतिक चौहद्दी को कमोबेश खुलकर स्वीकारने के बाद, उनका सामाजिक आधार और वोटबैंक सिकुड़ता जा रहा है, पर पूँजीवाद के लिए उनकी उपयोगिता अभी भी क़ायम है। किसी सशक्त, एकजुट क्रान्तिकारी विकल्प की अनुपस्थिति से आम जनता में जो निराशा है, उसके कारण वह सोचती है कि चलो, तबतक संसदीय वामपन्थी जो भी दो-चार आने की राहत दिला देते हैं, वही सही, क्योंकि क्रान्ति तो अभी काफ़ी दूर की बात है (या कि अब सम्भव नहीं है)। यानी आज भी संशोधनवाद जनता को अपने ऊपर पूँजीवाद को शासन करने की स्वीकृति देने के लिए तैयार करने का कार्य करता रहता है। इसे ही राजनीतिक वर्चस्व को स्वीकार करना कहते हैं।
ज्योति बसु इसी संशोधनवादी वाम राजनीति के एक महारथी थे। उनके जाने का दुख उनके संसदीय वामपन्थी साथी-सँघातियों को तो है ही, पूँजीवाद के कट्टर हिमायतियों, बुर्जुआ थिंक टैंकों और रणनीतिकारों को भी है और सुधारवादी मानस वाले मधयवर्गीय प्रगतिशीलों को भी। ज्योति बसु पुरानी पीढ़ी के संशोधनवादी थे। बुद्धदेव, सीताराम येचुरी, नीलोत्पल बसु और विजयन मार्का नये ज़माने वालों के मुकाबले वे ज्यादा खाँटी और पुराने फ्कम्युनिस्टी'' रंग ढंग वाले दिखते थे। पहले कभी गोपालन, सुन्दरैया, प्रमोद दासगुप्त, जैसों के मुक़ाबले ज्योति बसु ही फ्मॉडर्न'' माने जाते थे। मज़ाक में लोग उन्हें फ्पार्टी का उत्ताम कुमार'' भी कहते थे। ज्योति बसु संसदीय वामपन्थ की अधाोमुखी यात्राा के कई दौरों के साक्षी थे। तीन दशक पहले तक पार्टी में उन्हें सिद्धान्तकार और संगठनकर्ता का दर्जा, देश स्तर पर तो दूर, बंगाल स्तर पर भी हासिल नहीं था। बासवपुनैया, प्रमोद दासगुप्त, सुन्दरैया आदि की यह छवि थी। ज्योति बसु चुनावी राजनीति के स्टार थे, एक दक्ष राजनेता (स्टेट्समैन), कूटनीतिज्ञ (डिप्लोमैट) और प्रशासक थे। पंजाब के फ्जत्थेदार कॉमरेड'' हरकिशन सिंह सुरजीत घनघोर व्यवहारवादी (प्रैग्मेटिक) और जोड़तोड़ में माहिर-तिकड़मी राजनीतिज्ञ थे।
ज्योति बसु का जन्म 1914 में बंगाल के एक उच्च मधयवर्गीय कुलीन परिवार में हुआ था। 1935 में वे बैरिस्टरी की पढ़ाई करने लंदन गये। इस दौरान वे प्राय: लंदन स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स जाकर प्रख्यात सामाजिक जनवादी विद्वान हेराल्ड लास्की के भाषण सुनते थे। लास्की के विचारों ने ही उनके भीतर समाजवादी रुझान पैदा किया। 1937 में वे राष्ट्रवादी छात्राों के साथ 'इण्डिया लीग' और 'लंदन मजलिस' संस्थाओं में सक्रिय रहे। नेहरू, सुभाष और अन्य भारतीय नेताओं को लेबर पार्टी के नेताओं और समाजवादी नेताओं से मिलवाने का काम भी उन्होंने किया। इसी बीच 1939 में वे रजनी पाम दत्ता के सम्पर्क में आये, जो ब्रिटिश कम्युनिस्ट पार्टी के एक शीर्ष नेता थे। कम्युनिस्ट इण्टरनेशनल की भारत और उपनिवेश- विषयक नीतियों की व्याख्या करते हुए वे भारत और ब्रिटेन के पार्टी मुखपत्राों में लेख लिखा करते थे और प्राय: उनमें अपनी ओर से कुछ संशोधनवादी छौंक-बघार लगा दिया करते थे। वे एक अभिजात कम्युनिस्ट थे, जिनकी संशोधनवादी रुझानें उस समय भी थीं, जब ब्रिटेन की कम्युनिस्ट पार्टी का रंग अभी बदला नहीं था। बाद में संशोधनवाद की ओर पार्टी को धाकेलने में उनकी अग्रणी भूमिका रही थी। तो ऐसे व्यक्ति थे ज्योति बसु के राजनीतिक पथप्रदर्शक। दरअसल अपनी पीढ़ी के बहुतेरे उच्च मधयवर्गीय युवाओं की तरह ज्योति बसु भी एक रैडिकल राष्ट्रवादी थे जिन्हें समाजवाद के नारे आकृष्ट तो करते थे, लेकिन कम्युनिज्म की क्रान्तिकारी अन्तर्वस्तु को वे कभी भी आत्मसात नहीं कर पाये। चूँकि कम्युनिस्ट पार्टी भी उस समय अभी समाजवाद के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्रीय मुक्ति के लिए और जनवादी क्रान्ति के लिए लड़ रही थी, इसलिए बहुतेरे ऐसे रैडिकल जनवादी राष्ट्रवादी युवा उस समय पार्टी में शामिल हो रहे थे, जिन्हें कांग्रेस की समझौतापरस्ती की राजनीति रास नहीं आ रही थी। बहरहाल, युवा ज्योति बाबू में तब नौजवानी का जोश, वफुर्बानी का जज्बा और आदर्शवाद की भावना तो थी ही। स्वदेश-वापसी के बाद, वक़ालत करने के बजाय उन्होंने पेशेवर क्रान्तिकारी का जीवन चुना और मज़दूरों के बीच काम करने लगे। ग़ौरतलब है कि यह भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का वह दौर था जब पी.सी. जोशी के नेतृत्व में दक्षिणपन्थी भटकाव पार्टी पर हावी था। 1941 में ज्योति बसु ने बंगाल-असम रेलवे के मज़दूरों के बीच काम किया और उनके यूनियन सेक्रेटरी भी रहे। कुछ समय तक उन्होंने बंदरगाह और गोदी मज़दूरों के बीच भी काम किया।
कम्युनिस्ट पार्टी क़ानूनी घोषित की जाने के बाद 1943 में जब उसकी पहली कांग्रेस हुई तो उसमें ज्योति बसु प्रान्तीय संगठनकर्ता चुने गये। फ़िर चौथे राज्य सम्मेलन में उन्हें राज्य कमेटी में चुना गया। 1946 से देश एक ऐसे संक्रमण काल से गुज़रने लगा था, जिसमें प्रचुर क्रान्तिकारी सम्भावनाएँ निहित थीं। नौसेना विद्रोह, देशव्यापी मज़दूर हड़तालें, तेलंगाना-तेभागा-पुनप्रा वायलार के किसान संघर्ष ऌन ऐतिहासिक घटनाओं ने अगले तीन-चार वर्षों के दौरान पूरे देश को हिला रखा था। अपनी विचारधारात्मक कमज़ोरी, नेतृत्व में एकजुटता के अभाव और ढीले-ढाले सांगठनिक ढाँचे के कारण पार्टी इस निर्णायक घड़ी में पहल अपने हाथ में लेने में पूरी तरह विफ़ल रही (ऐसे अवसर वह पहले भी गँवा चुकी थी)। राष्ट्रीय आन्दोलन को नेतृत्व देने वाला बुर्जुआ वर्ग जनता की आकांक्षाओं के साथ विश्वासघात करते हुए साम्राज्यवादियों के साथ समझौते के साथ बुर्जुआ शासन की पूर्वपीठिका तैयार कर रहा था। बेशुमार साम्प्रदायिक ख़ून-ख़राबे के बाद देश का विभाजन हो रहा था। ऐसी राजनीतिक आज़ादी मिल रही थी जो अधाूरी और खण्डित थी। साम्राज्यवाद से निर्णायक विच्छेद के बजाय उसके आर्थिक हितों की सुरक्षा की गारण्टी दी जा रही थी। रैडिकल भूमि सुधार के मामले में भी कांग्रेस के विश्वासघात के संकेत मिल चुके थे। सार्विक मताधिकार के आधार पर चुने जाने के बजाय महज 12 फ़ीसदी आबादी द्वारा चुनी गयी संविधान सभा अत्यन्त सीमित जनवादी अधिकार देने वाला (और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें भी छीन लेने के इन्तज़ामों से लैस) वाग्जालों से भरा संविधान बना रही थी।
इस संक्रमण काल में कम्युनिस्ट पार्टी कन्फ़्रयूज़ थी, अनिर्णय का शिकार थी। रही-सही कसर रणदिवे की फ्वामपन्थी'' दुस्साहसवादी लाइन ने पूरी कर दी। नेहरू की भेजी हुई भारतीय पफौजों ने तेलंगाना किसान संघर्ष को कुचल दिया। लम्बी कमज़ोरियों और भूल-ग़लतियों के सिलसिले ने पार्टी को उसकी तार्किक परिणति तक पहुँचा दिया। तेलंगाना पराजय के बाद पार्टी पूरी तरह से संशोधनवादी हो गयी। चुनावी वामपन्थ का ज़माना आ गया। ज्योति बसु इस दौरान क्या कर रहे थे! किसान संघर्षों और जुझारू मज़दूर आन्दोलन को क्रान्तिकारी दिशा देने की किसी कोशिश के बजाय, पार्टी के निर्णय का पालन करते हुए उन्होंने 1946 की प्रान्तीय विधायिका का चुनाव लड़ा, रेलवे कांस्टीच्युएंसी से (सीमित मताधिकार के आधार पर), और विजयी रहे। उसी वर्ष भीषण साम्प्रदायिक दंगों के दौरान गाँधीजी जब बंगाल गये तो ज्योति बसु उनसे मिले और उनकी सलाह से एक शान्ति कमेटी बनायी और शान्ति मार्च निकाला। तेलंगाना किसान संघर्ष को लेकर पार्टी में जो कई लाइनों का संघर्ष था, उसमें उनकी कोई भूमिका नहीं थी। 1952 में जब पहले आम चुनाव हुए, तब वे बंगाल विधानसभा के सदस्य चुने गये और विधान चन्द्र राय की कांग्रेसी सरकार के शासनकाल के दौरान विपक्ष के नेता रहे। तबसे लेकर, सन् 2000 तक, 1972-77 की समयावधि को छोड़कर ज्योति बसु लगातार बंगाल की विधानसभा के लिए चुने जाते रहे। संसदीय राजनीति ही आधी शताब्दी तक उनका कार्यक्षेत्रा बनी रही। 1951 में वे पार्टी के बांग्ला मुखपत्रा 'स्वाधीनता' के सम्पादक-मण्डल के अधयक्ष चुने गये। 1953 में वे राज्य कमेटी के सचिव चुने गये। 1954 की मदुरै पार्टी कांग्रेस में वे केन्द्रीय कमेटी में और फ़िर पालघाट कांग्रेस में सेक्रेटेरियट में चुने गये। 1958 में अमृतसर की जिस विशेष कांग्रेस ने सोवियत पार्टी की बीसवीं कांग्रेस की ख्रुश्चेवी संशोधनवादी लाइन को सर्वसम्मति से स्वीकार किया था, उसी कांग्रेस में ज्योति बसु राष्ट्रीय परिषद में चुने गये थे। 1964 में जब भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का भाकपा और माकपा में विभाजन हुआ, तो यह संशोधनवाद और क्रान्तिकारी कम्युनिज्म के बीच का विभाजन नहीं था। वह विभाजन वस्तुत: संशोधनवाद और नवसंशोधनवाद के बीच था, नरमपन्थी संसदीय वामपन्थ और गरमपन्थी संसदीय वामपन्थ के बीच था, अर्थवाद और जुझारू अर्थवाद के बीच था। डांगे-राजेश्वर राव गुट (भाकपा) ख्रुश्चेवी संशोधनवाद का पूर्ण समर्थक था और नेहरूवादी फ्समाजवाद'' को प्रगतिशील राष्ट्रीय बुर्जुआ की नीति मानकर कांग्रेस का पुछल्ला बनने को तैयार था। विरोधी गुट (माकपा) ज्यादा शातिर संशोधनवादी था। माकपा नेतृत्व ख्रुश्चेवी संशोधनवाद की आलोचना करता था, लेकिन साथ ही चीन की पार्टी को भी अतिवाद का शिकार मानता था। सत्तारूढ़ सोवियत पार्टी को वह संशोधनवादी, लेकिन राज्य को समाजवादी मानता था। इस तर्क से कालान्तर में राज्य का समाजवादी चरित्रा भी समाप्त हो जाना चाहिए था, पर इसके उलट, माकपा ने कुछ ही वर्षों बाद सोवियत पार्टी को भी बिरादर पार्टी मानना शुरू कर दिया। माकपा नेतृत्व नेहरू सरकार को साम्राज्यवाद का जूनियर पार्टनर बन चुके इजारेदार पूँजीपति वर्ग का प्रतिनिधि मानकर उनके विरुद्ध राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा बनाकर संघर्ष करने की बात करता था।
माकपा का चरित्रा हालाँकि उसकी संसदीय राजनीति ने बाद में एकदम नंगा कर दिया, लेकिन 1964 में अपने गरम तेवर दिखाकर क्रान्तिकारी क़तारों के बड़े हिस्से को अपने साथ लेने में वह सफ़ल हो गयी। पार्टी संगठन के लेनिनवादी उसूलों के हिसाब से देखें तो माकपा का संशोधनवादी चरित्रा 1964 से ही एकदम साफ़ था। 1951 से जारी पार्टी के एकदम खुले, क़ानूनी, संसदीय चरित्रा और कार्यप्रणाली को माकपा ने यथावत् जारी रखा। पार्टी सदस्यता की प्रकृति रूस के मेंशेविकों से भी गयी-गुज़री थी। अमृतसर कांग्रेस में पार्टी संविधान में किये गये बदलाव को 1964 में यथावत् क़ायम रखा गया। पार्टी के लोक जनवादी क्रान्ति के कार्यक्रम के हिसाब से दीर्घकालिक लोकयुद्ध ही क्रान्ति का मार्ग हो सकता था, पर इसके उल्लेख से बचकर पार्टी कार्यक्रम में छलपूर्ण भाषा में फ्संसदीय और ग़ैर-संसदीय रास्ते'' का उल्लेख किया गया। कोई भी क्रान्तिकारी पार्टी बुर्जुआ संसदीय चुनावों का महज रणकौशल के रूप में इस्तेमाल करती है। संसदीय मार्ग को ग़ैर-संसदीय मार्ग के समकक्ष रखना अपने आप में संशोधनवाद है। 1967 में और 1969 में माकपा यही कहती थी कि वह संसद-विधानसभा का इस्तेमाल रणकौशल (टैक्टिक्स) के रूप में ही करती है। लेकिन 33 वर्षों तक बुर्जुआ व्यवस्था के अन्तर्गत बंगाल में शासन करते हुए (इनमें से 23 वर्षों तक ज्योति बसु के मुख्यमन्त्रिात्व में) उसने बुर्जुआ नीतियों को भरपूर वफ़ादारी के साथ लागू किया है और वर्ग संघर्ष की तैयारी के लिए चुनावों के टैक्टिकल इस्तेमाल के बजाय हर जनान्दोलन को कुचलने के लिए राज्यतन्त्र का बर्बर इस्तेमाल किया है। ज्योति बसु को इस साफ़गोई के लिए सराहा जाना चाहिए कि 1977 से 1990 के बीच दो-तीन बार उन्होंने कहा था कि 'हम पूँजीवाद के अन्दर एक राज्य में सरकार चला रहे हैं, समाजवाद नहीं ला रहे हैं।' माकपा पिछले दो-तीन दशकों से चुनाव के 'टैक्टिकल इस्तेमाल' वाला जुमला भूले से भी नहीं दुहराती। अब वह न केवल ख्रुश्चेवी शान्तिपूर्ण संक्रमण के सिद्धान्त को पूरी तरह से मौन स्वीकृति दे चुकी है और उसके और भाकपा के बीच व्यवहारत: कोई अन्तर नहीं रह गया है, बल्कि उसका आचरण एक निहायत भ्रष्ट एवं पतित सामाजिक जनवादी पार्टी जैसा ही है। भ्रष्टाचार का दीमक उसमें अन्दर तक पैठ चुका है (हालाँकि अन्य बुर्जुआ पार्टियों से फ़िर भी काफ़ी कम है) और बंगाल में राज्य मशीनरी के साथ माकपाई गुण्डाें-मस्तानों के समानान्तर तन्त्र की मौजूदगी ने सोशल फ़ासिस्ट दमन का माहौल बना रखा है।
जब माकपा-भाकपा का बँटवारा हो रहा था तो कुछ मधयमार्गी भी थे जो बीच में डोल रहे थे। फ़िर इनमें से कुछ भाकपा में गये कुछ माकपा में। जैसे, भूपेश गुप्त भाकपा में गये, ज्योति बसु माकपा में। ज्योति बसु शुरू से ही एक घुटे-घुटाये संसदीय वामपन्थी थे। 1967 में नक्सलबाड़ी किसान उभार के बाद एक नये धा्रुवीकरण की शुरुआत हुई। कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी कतारें भारी तादाद में माकपा से निकलकर नक्सलबाड़ी के झण्डे तले इकट्ठा होने लगीं। नक्सलबाड़ी पहले एक क्रान्तिकारी जनसंघर्ष के रूप में पूफटा लेकिन 1969 आते-आते उसपर चारु मजुमदार की फ्वामपन्थी'' आतंकवादी लाइन हावी हो गयी और फ़िर इसी लाइन पर भाकपा (मा.ले.) का निर्माण्ा हुआ। जो लोग आतंकवादी लाइन के विरोधी थे, वे भी राष्ट्रीय परिस्थितियों और कार्यक्रम की ग़लत समझ के कारण कोई क्रान्तिकारी विकल्प नहीं दे सके और यह पूरी धारा बिखराव का शिकार हो गयी। लेकिन 1967-68 में तो नक्सलबाड़ी उभार ने माकपा के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा कर दिया था।
1967 में बंगाल में संयुक्त मोर्चे की जो सरकार बनी थी, उसमें माकपा शामिल थी। ज्योति बसु उप-मुख्यमन्त्राी तथा वित्ता और परिवहन के मन्त्राी थे। माकपा ने सरकार से बाहर आकर नक्सलबाड़ी किसान उभार को समर्थन देने के बजाय, पहले तो वहाँ के स्थानीय पार्टी नेताओं एवं कतारों को समझाने-बुझाने का प्रयास किया। फ़िर सभी को पार्टी से बाहर किया गया और राज्य की सशस्त्रा पुलिस मशीनरी और (राज्य सरकार की अनुमति से) केन्द्रीय सशस्त्रा बलों का इस्तेमाल करके नक्सलबाड़ी आन्दोलन को बेरहमी से कुचल दिया गया। इसमें ज्योति बसु की उप-मुख्यमन्त्राी के रूप में अहम भूमिका थी। इस समय तक आन्दोलन पूरे देश में पफैल चुका था। हर राज्य में माकपा टूट रही थी। मा-ले पार्टी के गठन की प्रक्रिया शुरू हो रही थी। माकपा नेतृत्व ने सभी नक्सलबाड़ी समर्थकों को पार्टी से निकाल बाहर किया। 1969 में प. बंगाल में पुन: संयुक्त मोर्चे की जो सरकार बनी, उसमें भी ज्योति बसु उप-मुख्यमन्त्राी थे और साथ ही गृह, पुलिस और सामान्य प्रशासन विभाग भी उन्हीं के पास था। इस समय नक्सलबाड़ी तो कुचला जा चुका था, पर बंगाल के कई इलावफे धाधाक रहे थे। फ्वामपन्थी'' आतंकवादी कार्रवाइयाँ भी शुरू हो चुकी थीं। ज्योति बसु ने इस बार प्रतिरोधा को कुचलने के लिए पुलिस मशीनरी का बर्बर और बेधाड़क इस्तेमाल किया। 1972 के चुनावों में ज़बर्दस्त धाँधाली के बाद बंगाल में कांग्रेस की सरकार बनी। सिद्धार्थ शंकर रे मुख्यमन्त्राी बने। पूरे देश में तो आपातकाल जून 1975 में लगा, लेकिन बंगाल में नक्सलवादियों के दमन के नाम पर यन्त्राणा, फ़र्ज़ी मुठभेड़ों के ज़रिये फ़ासिस्ट पुलिस राज्य सिद्धार्थ शंकर रे ने 1972 में ही क़ायम कर दिया था। माकपा ने 1972 से 1977 तक विधानसभा का बहिष्कार किया। 1977 में आपातकाल हटने के बाद केन्द्र में जनता पार्टी शासन स्थापित हुआ और बंगाल में वाम मोर्चे का शासन क़ायम हुआ जो आज तक जारी है। ज्योति बसु मुख्यमन्त्राी बने और 2000 तक इस पद पर रहते हुए एक कीर्तिमान स्थापित किया। यह इतिहास का स्मरणीय तथ्य है कि सिद्धार्थ शंकर रे के शासनकाल के पहले, गृह एवं पुलिस मन्त्राालय सँभालते हुए नक्सलवाद के दमन के नाम पर पुलिस राज्य क़ायम करने का काम ज्योति बसु ने भी किया था।
1977 में ज्योति बसु ने जब बंगाल का मुख्यमंत्रिात्व सँभाला उस समय उनके सामने नक्सलबाड़ी की चुनौती नहीं थी। लेकिन नक्सलबाड़ी की एक नसीहत सामने थी, जिसपर सभी बुर्जुआ अर्थशास्त्राी, राजनीतिज्ञ और संशोधनवादी सहमत थे। सबकी कमोबेश एक ही राय थी और वह यह कि यदि नक्सलबाड़ी जैसे विस्पफोटों से और उसके फ्सम्भावित'' भयावह नतीजों से बचना है तो बुर्जुआ भूमि सुधारों की गति थोड़ी और तेज़ करनी होगी। ज्योति बसु ने इसी काम को 'आपरेशन बर्गा' के रूप में अंजाम दिया। आज माकपाई झाल-करताल लेकर 'ऑपरेशन बर्गा' का कीर्तन करते हैं। 'ऑपरेशन बर्गा' कोई क्रान्तिकारी भूमि सुधार नहीं था। वह ''ऊपर से किया गया,'' प्रशियाई टाइप, स्तॉलिपिन सुधार टाइप, मरियल बुर्जुआ भूमि सुधार कार्यक्रम था, जिसने आंशिक तौर पर भूमि के मालिकाने के सवाल को हल करके बंगाल की खेती में क्रमिक पूँजीवादी विकास की ज़मीन तैयार की और वहाँ कुलकों-पूँजीवादी किसानों के पैदा होने का आधार बनाया। ऐसे भूमि सुधार बहुतेरे अन्य प्रान्तों में हो चुके थे। बंगाल पीछे छूटा हुआ था। यदि रैडिकल चरित्रा की ही बात की जाये तो छठे दशक के शुरू में ही, अपने पहले शासनकाल के दौरान शेख़ अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर में ज्यादा रैडिकल बुर्जुआ भूमि-सुधार कार्यक्रम लागू किया था।
1977 तक भारत का पूँजीवाद काफ़ी मज़बूत हो चुका था और कृषि के पूँजीवादीकरण की प्रक्रिया को तेज़ करके, रहे-सहे र्अद्ध-सामन्ती अवशेषों को समाप्त करके एक व्यापक राष्ट्रीय बाज़ार का निर्माण करना उसकी ज़रूरत थी। ज्योति बसु ने 'ऑपरेशन बर्गा' के द्वारा पूँजीवादी भूमि-सुधार के इसी कार्यक्रम को कुशलतापूर्वक लागू किया और भारतीय पूँजीवाद की ऐतिहासिक सेवा की। 'ऑपरेशन बर्गा' ने काश्तकार किसानों को आंशिक मालिकाना हक़ देकर पूँजीवादी खेती के विकास के साथ ही इन नये छोटे-बड़े मालिक किसानों में माकपा का नया सामाजिक आधार और वोट बैंक तैयार किया। गाँवों में जो बड़े मालिक किसानों का ताक़तवर हिस्सा पैदा हुआ, उसे राजनीतिक सत्ता में (आर्थिक ताक़त के अनुरूप) भागीदारी भी चाहिए थी। यह उसे एक ओर माकपा पार्टी तन्त्र के स्थानीय मनसबदार के रूप में हासिल हुआ (बंगाल में माकपा की पार्टी मशीनरी प्रशासन मशीनरी के साथ मिलकर काम करती है) और दूसरी ओर पंचायती राज ने उसे लूटने-खाने और शासन करने का मौक़ा दिया। पूँजीवादी पंचायती राज का 'ट्रेण्ड-सेटर' प्रयोग वास्तव में ज्योति बसु ने किया था जिसे राजीव गाँधी शासन काल के दौरान कांग्रेस ने अपना लिया था (हालाँकि उतने प्रभावी ढंग वह इसे लागू नहीं कर पायी)।
बंगाल के गाँवों में पूँजीवादी विकास का सिलसिला जब कुछ और आगे बढ़ा तो जो छोटे मालिक किसान पूँजीवादी शोषण का शिकार हो रहे थे, उनका धीरे-धीरे माकपा व वाम मोर्चा से मोहभंग होने लगा। माकपा के स्थानीय कार्यकर्ताओं (जो प्राय: नवधानिक कुलक या ग्रामीण मधयवर्ग के लोग थे) की गुण्डागर्दी और भ्रष्टाचार ने इसमें विशेष भूमिका निभायी। उधार नवधानिक कुलकों का एक हिस्सा भी लूट के माल और स्थानीय सत्ता के बँटवारे के बढ़ते अन्तरविरोधों के चलते माकपा से दूर हटा। गाँवों में इन्हीं के बीच तृणमूल कांग्रेस ने (और कहीं-कहीं कांग्रेस ने भी) अपना नया वोट बैंक तैयार किया है।
वर्ष 1977 में ज्योति बसु के नेतृत्व में वाम मोर्चा सरकार की विभिन्न सुधारवादी कार्रवाइयों ने नगरों-महानगरों में मधय वर्ग को विशेष तौर पर अपनी ओर खींचा। संगठित मज़दूरों को भी शुरू में कुछ आर्थिक लाभ मिले। सबसे बड़ी बात यह थी सिद्धार्थ शंकर रे के काले आतंक राज को भूलने और कांग्रेस को माफ़ करने के लिए मधयवर्ग और मज़दूर कत्ताई तैयार नहीं थे। यही कारण था कि जब ज्योति बसु सरकार के बुर्जुआ सुधारों का 'स्कोप' समाप्त हो गया, शासन-प्रशासन में बढ़ता भ्रष्टाचार साफ़ दीखने लगा और माकपा के स्थानीय नेताओं की दादागिरी भी बढ़ने लगी, तब भी बंगाल की जनता विशेषकर शहरी मधय वर्ग और औद्योगिक मज़दूर उसे मजबूरी का विकल्प मानते रहे। बंगाल के शहरों में जनवादी चेतना अधिक रही है और सिद्धार्थ शंकर रे के शासनकाल को याद करके बंगाल की जनता सोचती रही कि जनवादी अधिकारों के नज़रिये से माकपा शासन को बनाये रखना उसकी विवशता है।
इस बीच ज्योति बसु, माकपा और वाम मोर्चे का सामाजिक जनवादी चरित्रा ज्यादा से ज्यादा नंगा होता चला गया। भद्रपुरुष ज्योति बाबू बार-बार मज़दूरों को हड़तालों से दूर रहने और उत्पादन बढ़ाने की राय देने लगे, जबकि मज़दूरों की हालत लगातार बद से बदतर होती जा रही थी। ज्योति बसु विदेशी पूँजी को आमन्त्रिात करने के लिए बार-बार पश्चिमी देशों की यात्राा पर निकलने लगे (कभी छुट्टियाँ बिताने तो कभी आर्थिक-तकनीकी मदद के लिए 1990 तक रूस और पूर्वी यूरोप तो जाते ही रहते थे)। देशी पूँजीपतियों को पूँजी-निवेश के लिए पलक-पाँवड़े बिछाकर आमन्त्रिात किया जाने लगा। देश के तमाम बड़े पूँजीपति (विदेशी कम्पनियाँ भी) पूँजी निवेश के लिए बंगाल के परिवेश को अनुकूल बताने लगे। दिक्वफत अब उन्हें हड़तालों से नहीं थी, बल्कि माकपा के उन ट्रेड यूनियन क्षत्रापों से थी जो मज़दूरों से वसूली करने के साथ ही मालिकों से भी कभी-कभी कुछ ज्यादा दबाव बनाकर वसूली करने लगते थे।
जब 1991 से नरसिंह राव की सरकार ने उदारीकरण-निजीकरण की नीतियों की शुरुआत की तो माकपा देश स्तर पर तो उसका विरोध कर रही थी, लेकिन बंगाल में ज्योति बसु की सरकार उन्हीं नीतियों को लागू कर रही थी। चीन का फ्बाज़ार समाजवाद'' माकपा को नवउदारवादी लहर में बहने का तर्क दे रहा था, दूसरी ओर उदारीकरण-लहर को कुछ ''मानवीय चेहरा'' देने मात्रा की सिफ़ारिश करते हुए माकपा 'सेफ़्टी वॉल्व' का और पैबन्दसाज़ी का अपना पुराना सामाजिक जनवादी दायित्व भी निभा रही थी। गत् शताब्दी के अन्तिम दशक के उत्तारर्ाद्ध तक माकपा की नीतियों से मज़दूर वर्ग और शहरी निम्न मधयवर्ग को अब आंशिक सुधार की भी उम्मीद नहीं रह गयी थी। पूँजी निवेश से रोज़गार पैदा होने की उम्मीदें मिट्टी में मिल चुकी थीं। कलकत्ता के औद्योगिक मज़दूरों की स्थिति अन्य औद्योगिक केन्द्रों से भी बदतर थी।
माकपा ने मुहल्ले-मुहल्ले तक, मज़दूर बस्तियों से लेकर दुर्गापूजा समितियों तक अपने मस्तान नुमा कार्यकर्ताओं का ऐसा नेटवर्क तैयार कर लिया था कि अस्पताल में भरती होने से लेकर स्कूल में एडमिशन तक का काम उनके बिना नहीं हो सकता था। माकपा प्रभुत्व वाली मज़दूर यूनियनों और छात्रा यूनियनों के प्रभाव क्षेत्रा में राजनीतिक पैठ की किसी कोशिश को गुण्डागर्दी से दबा दिया जाता था। इसी प्रकार का माफ़िया तन्त्र गाँवों में पार्टी दफ़्रतरों और पंचायती राज संस्थाओं के इर्द-गिर्द निर्मित हो चुका था। यह सब कुछ ज्योति बसु के ही शासनकाल के दौरान हुआ था। इसके बावजूद विशेषकर पिछले दो या तीन चुनावों में वाममोर्चा यदि जीता तो उसका मुख्य कारण था सी.पी.एम. के पार्टी माफ़िया तन्त्र का आतंककारी, प्रभावी नेटवर्क और किसी कारगर बुर्जुआ चुनावी विकल्प का अभाव। तृणमूल ने एक हद तक स्वयं वैसा ही नेटवर्क खड़ा करके (लोहे को लोहे से काटने की नीति अपनाकर), गाँवों में मालिक किसानों के प्रतिर्स्पद्धी गुटों और माकपा से निराश ग़रीब किसानों को साथ लेकर तथा कांग्रेस के साथ मोर्चा बनाकर जब प्रभावी चुनौती पेश की है तो प्रबुद्ध शहरी मधयवर्ग का बड़ा हिस्सा भी इधार आकृष्ट हुआ है। सिंगूर और नन्दीग्राम ने माकपा की मिट्टी और अधिक पलीद करने का काम किया है। चुनावी राजनीति के दायरे में पहली बार माकपा के सितारे गर्दिश में नज़र आ रहे हैं। इस दायरे के बाहर क्रान्तिकारी विकल्प की तलाश करते हुए मेहनतकश ग्रामीण आबादी का सबसे तबाह हिस्सा और रैडिकल शहरी युवाओं का एक हिस्सा ''वामपन्थी'' दुस्साहसवादी राजनीति की ओर मुड़ा है। तीसरी ओर, औद्योगिक मज़दूरों और रैडिकल छात्रों-युवाओं का एक हिस्सा क्रान्तिकारी जन राजनीति की नयी दिशा और नये रूपों के सन्धान की ओर उन्मुख हुआ है। बंगाल की राजनीति आज एक मोड़ पर खड़ी है। आगे बदला हुआ परिदृश्य चाहे जैसा भी हो, इतना तय है कि माकपा के ''सुनहरे दिन'' अब बीत चुके हैं।
सच पूछें, तो इस पराभव की शुरुआत तो ज्योति बसु के शासन काल के दौरान ही हो चुकी थी। यूँ तो स्वास्थ्य कारणों से 2000 में उन्होंने मुख्यमन्त्राी पद छोड़ा था, लेकिन इज्ज़त बचाकर निकल लेने के लिए, ससम्मान मंच से विदा होने के लिए, उन्होंने बिल्कुल सही समय का चुनाव किया था। व्यक्तिगत तौर पर एक कसक रह गयी थी 1996 में वी.पी. सिंह द्वारा प्रस्ताव रखने के बावजूद माकपा ने उन्हें देश का प्रधानमन्त्री बनने से रोक दिया था। इसके पहले 1989 में भी अरुण नेहरू और चन्द्रशेखर ने वी.पी. सिंह की जगह उन्हें प्रधानमन्त्री बनने का प्रस्ताव रखा था, पर तब वे खुद ही नहीं चाहते थे। 1996 में उनका कैल्कुलेशन यह था कि यदि वे प्रधानमन्त्री बन जायेंगे तो अन्य बुर्जुआ पार्टियाँ बहुत दिनों तक तो सरकार चलने नहीं देंगी। इस तरह मरने से पहले प्रधानमन्त्री बनने की उनकी निजी साधा भी पूरी हो जायेगी और सत्ताच्युत होने के बाद यह कहकर ''शहीद'' बनने का मौक़ा मिल जायेगा कि जनहित की नीतियाँ लागू करते ही साम्राज्यवादियों-पूँजीपतियों और बुर्जुआ पार्टियों ने उनकी सरकार गिरा दी। पार्टी में प्रकाश करात के हावी गुट का कैल्कुलेशन यह था कि केन्द्र स्तर पर यदि दो-ढाई वर्षों तक भी सरकार चलती रही तो नवउदारवादी नीतियों को लागू करने के चलते माकपा की लँगोटी उतर जायेगी और बची-खुची इज्ज़़त भी नीलाम हो जायेगी। अब इनमें से कौन ज्यादा सही सोच रहा था, यह अटकल लगाना हमारा काम नहीं है। जो भी हो, पूँजीवादी संसदीय जनवाद की इतनी सेवा करने के बावजूद ज्योति बसु को यदि प्रधानमन्त्री बनने की साधा लिये-लिये इस दुनिया से जाना पड़ा, यदि अपने ही ''कामरेडों'' ने किये-दिये पर पानी फ़ेर दिया, तो वे कर भी क्या सकते थे! ज्यादा से ज्यादा भड़ास निकाल सकते थे और 1996 के पार्टी के निर्णय को ''ऐतिहासिक भूल'' बताकर उन्होंने यही किया था।
ज्योति बसु प्रधानमन्त्री भले ही नहीं बन सके, उन्हें उनके अवदानों के लिए न केवल अपने संसदीय वामपन्थी साथियों से, बल्कि बुर्जुआ नेताओं, विचारकों और बुद्धजिीवियों से तथा बुर्जुआ मीडिया से भरपूर सम्मान मिला। उनके निधन पर सभी ने शोकविह्नल होकर उन्हें याद किया। क्रान्तिकारी उथल-पुथल के तूफ़ानों से डरने वाले, भलेमानस मधयवर्ग के बहुतेरे शान्तिवादी, पैबन्दवादी, करुणामय हृदय वाले बुद्धिजीवियों ने भी पुरानी पीढ़ी के इस संसदीय वामपन्थी महारथी को भावुक होकर श्रद्धांजलि दी।
Read more...
माकपा, भाकपा, आर.एस.पी., फ़ॉरवर्ड ब्लॉक आदि रंग-बिरंगी चुनावी वामपन्थी पार्टियों के नेताओं के अतिरिक्त प्रधानमन्त्री और सोनिया गाँधी से लेकर सभी बुर्जुआ दलों के नेताओं ने कलकत्ता पहुँचकर ज्योति बसु को श्रद्धांजलि दी। कई पूँजीपतियों ने बंगाल में पूँजी लगाने में उनके सहयोग को भावविह्नल होकर याद किया। टाटा, बिड़ला, जैन आदि सभी छोटे-बड़े पूँजीपति घरानों के छोटे-बड़े अंग्रेज़ी-हिन्दी अख़बारों ने उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए स्मृति लेख लिखे। कुछ टुटपूँजिया टिप्पणीकारों ने आश्चर्य प्रकट किया कि इतना भलेमानस आदमी कम्युनिस्ट क्यों और कैसे था? किसी ने लिखा कि वे भले आदमी पहले थे और कम्युनिस्ट बाद में। समझदार बुर्जुआ टिप्पणीकारों ने ऐसी बातें नहीं की। वे जानते हैं कि ज्योति बसु जैसे संसदीय कम्युनिस्टों की इस व्यवस्था को कितनी ज़रूरत होती है! यदि उनके ऊपर ''कम्युनिस्ट'' का लेबल ही नहीं रहेगा, तो वे पूँजीवादी व्यवस्था के लिए उतने उपयोगी भी नहीं रहे जायेंगे।
ज्योति बसु एक 'भद्रलोक' (जेण्टलमैन) कम्युनिस्ट थे शालीन, नफ़ीस, सुसंस्कृत। वे क्रान्ति और संघर्ष की वे बातें नहीं करते थे, जो खाते-पीते फ्जेण्टलमैन'' सुधारवादी मधयवर्ग को भाती नहीं। ज्योति बसु की जीवन-शैली, कार्य-शैली उनकी राजनीति के सर्वथा अनुरूप थी। इसलिए फ्सामाजिक अशान्ति'' से भयाकुल रहने वाले मधयवर्ग के उन लोगों को और (आदतों एवं जीवनशैली में मधयवर्ग बन चुके) सपफेदपोश कुलीन मज़दूरों को वे काफ़ी भाते थे। जो दयालु, करुणामय और फ्शान्तिप्रिय'' मधयवर्गीय भलेमानस पूँजीवादी व्यवस्था को आमूल रूप से बदल डालने के फ्ख़तरनाक और जोखिम भरे झंझट'' से दूर रहकर इसी व्यवस्था को सुधारकर ग़रीब-ग़ुरबा की ज़िन्दगी में भी बेहतरी लाने के भ्रम में जीते हैं और ऐसा भ्रम पैदा करते हैं, जो लोग पूँजीवादी उत्पादन-प्रणाली के क्षुद्र रहस्य और पूँजीवादी राजनीतिक तन्त्र के अपरिवर्तनीय वर्ग-चरित्रा को समझे बिना यह सोचते रहते हैं कि यदि नेता भ्रष्टाचारी न हों और नौकरशाही- लालफ़ीताशाही न हो तो सबकुछ ठीक हो जायेगा, ऐसे भोले-भाले, नेकनीयत मधयवर्ग के लोगों को भी ज्योति बसु, नम्बूदिरिपाद, सुन्दरैया जैसे व्यक्तित्व बहुत भाते हैं। यह भी सामाजिक जनवाद या संशोधनवादी राजनीति की एक सफ़लता है।
ज्योति बसु सादगी भरा, लेकिन उच्च मधयवर्गीय कुलीन जीवन जीते थे, लेकिन उनपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया जा सकता। उनसे भी अधिक सादा जीवन माकपा के गोपालन, सुन्दरैया, नम्बूदिरिपाद, हरेकृष्ण कोन्नार, प्रमोद दासगुप्ता जैसे नेताओं का था। पर बुनियादी सवाल किसी नेता के सादगी और ईमानदारी भरे निजी जीवन का नहीं है। बुनियादी सवाल यह भी नहीं है कि वह नेता समाजवाद और कम्युनिज्म की बातें करता है। बुनियादी सवाल यह है कि क्या समाजवाद और कम्युनिज्म की उसकी बातों का वैज्ञानिक आधार है, क्या उसकी नीतियाँ एवं व्यवहार अमली तौर पर मज़दूर वर्ग को उसकी मुक्ति की निर्णायक लड़ाई की दिशा में आगे बढ़ाते हैं? सादा जीवन गाँधी का भी था और अपने बुर्जुआ मानवतावादी सिद्धान्तों पर उनकी निजी निष्ठा पर भी सन्देह नहीं किया जा सकता। उनके मानवतावादी यूटोपिया ने करोड़ों आम जनों को जागृत-सक्रिय किया, लेकिन उस यूटोपिया को अमल में लाने की हर प्रकार की कोशिश की अन्तिम परिणति पूँजीवादी सामाजिक-आर्थिक ढाँचे की स्थापना के रूप में ही सामने आनी थी। कहने का मतलब यह कि बुनियादी प्रश्न किसी के ईमानदार नैतिक जीवन और उसकी यूटोपियाई निजी निष्ठाओं का नहीं, बल्कि उसकी विचारधारात्मक-राजनीतिक वर्ग- अवस्थिति का होता है। एक सच्चा और ईमानदार व्यक्ति यदि बुर्जुआ राजनीति के दायरे में ही काम करता है, तो वह वस्तुगत रूप से बुर्जुआ वर्ग की ही सेवा करेगा और उसकी अच्छी छवि बुर्जुआ व्यवस्था के प्रति लोगों का विभ्रम मज़बूत बनाने में मददगार ही बनेगी। लेकिन चूँकि हमारे सामाजिक व्यवहार से ही हमारी चेतना निर्मित-अनुकूलित होती है, इसलिए एक ग़लत राजनीति को वस्तुगत तौर पर लागू करने वाले लोग कालान्तर में सचेतन तौर पर भी ग़लत हो जाते हैं और निजी जीवन के स्तर पर भी ढोंग-पाखण्ड, झूठ-फ़रेब और भ्रष्टाचार से लबरेज़ हो जाते हैं। संशोधनवादी पार्टियों के बहुतेरे पुराने नेता व्यक्तिगत तौर पर भ्रष्ट-पतित नहीं, बल्कि भद्र नागरिक थे। आज यह बात नहीं कही जा सकती। इन पार्टियों में ऊपर यदि भ्रष्ट-पतित लोगों की भरमार है, तो नीचे क़तारों में गली के गुण्डे-लपफंगे तक घुस गये हैं। इनका यह सामाजिक चारित्रिाक पतन सामाजिक जनवाद/ संशोधनवाद/संसदीय वामपन्थ के क्रमिक राजनीतिक पतन-विघटन की ही एक परिणति है, एक अभिव्यक्ति है और एक प्रतिबिम्ब है। सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के देशों में नकली समाजवाद का झण्डा (ख्रुश्चेव काल से सोवियत संघ ही संशोधनवादियों का मक्का था) 1990 में गिर गया। फ़िर चीन में 1976 में माओ की मृत्यु के बाद देघपन्थी संशोधनवाद की जो सत्ता क़ायम हुई थी, उसका फ्बाज़ार समाजवाद'' अब सरेबाज़ार अलफ़ नंगा खड़ा अपनी पूँजीवादी असलियत की नुमाइश कर रहा है। ऐसी सूरत में, दुनिया भर की रंग-बिरंगी ख्रुश्चेवी संशोधनवादी पार्टियों ने ज्यादा खुले तौर पर पूँजीवादी संसदीय राजनीति और अर्थवादी राजनीति की चौहद्दी को स्वीकार कर लिया है। अब उनका बात-व्यवहार एकदम खुले तौर पर (सारतत्व तो पहले से ही एक था) वैसा ही हो गया है जैसा कि 1910 के दशक में मार्क्सवाद से विपथगमन करने वाली काउत्सकीपन्थी सामाजिक जनवादी पार्टियों का रहा है। यूरोप से लेकर कई लातिन अमेरिकी देशों तक में लेबर पार्टियों और सोशलिस्ट पार्टियों का आचरण दक्षिणपन्थी बुर्जुआ पार्टियों जैसा हो गया है तथा ख्रुश्चेवी कम्युनिस्ट पार्टियों का आचरण लेबर और सोशलिस्ट पार्टियों जैसा हो गया है। भारत में कुछ पुराने समाजवादी फ़ासिस्ट भाजपा के साथ गाँठ जोड़ सरकारें चला रहे हैं, कुछ धानी किसानों-कुलकों की राजनीति कर रहे हैं तो कुछ अलग-अलग बुर्जुआ पार्टियों में घुल-मिल गये हैं। जो ख्रुश्चेवी और देंगपन्थी संशोधनवादी पार्टियाँ हैं, वे भूमण्डलीकरण की पूरी राजनीति एवं अर्थनीति को स्वीकारते हुए बस उसे कुछ फ्मानवीय चेहरा'' देने की बात करती हैं तथा सरपट उदारीकरण- निजीकरण की राह में कुछ स्पीड-ब्रेकर्स लगाने की बात करती हैं, ताकि मेहनतकश अवाम का पूँजीवादी व्यवस्था और संसदीय राजनीति के प्रति भरम बने रहे तथा निर्बाधा उदारीकरण- निजीकरण की भयंकर सामाजिक परिणतियाँ (बेशुमार छँटनी, बेरोज़गारी, विस्थापन, मज़दूरों के रहे-सहे अधिकारों एवं सामाजिक सुरक्षा का भी अपहरण, धानी-ग़रीब की बढ़ती खाई आदि) किसी क्रान्तिकारी तूफ़ान के उभार के लिए ज़रूरी सामाजिक दबाव न पैदा कर दें। इस तरह, अपनी छद्म वामपन्थी जुमलेबाज़ी को छोड़ देने और बुर्जुआ चेहरे से नक़ाब थोड़ा हटा देने के बावजूद, पूरी दुनिया की ही तरह, भारत की संशोधनवादी वामपन्थी पार्टियाँ अभी भी इस व्यवस्था की वफ़ादार सुरक्षा पंक्ति की, सामाजिक ताप पर ठण्डा पानी डालते रहने वाले पुफहारे की तथा जनाक्रोश के दाब को कम करने वाले सेफ़्रटीवॉल्व की भूमिका अत्यन्त कुशलतापूर्वक निभा रही हैं। उनके फ्कम्युनिज्म'' को लेकर जनता को कोई भ्रम नहीं रह गया है और इस मायने में उनकी एक भूमिका (भ्रमोत्पादक की भूमिका) तो समाप्त हो चुकी है, लेकिन फ्वाम'' सुधारवादी राजनीतिक शक्ति के रूप में पूँजीवाद की दूसरी सुरक्षा-पंक्ति के रूप में उनकी भूमिका अभी भी क़ायम है। नवउदारवाद की राजनीतिक चौहद्दी को कमोबेश खुलकर स्वीकारने के बाद, उनका सामाजिक आधार और वोटबैंक सिकुड़ता जा रहा है, पर पूँजीवाद के लिए उनकी उपयोगिता अभी भी क़ायम है। किसी सशक्त, एकजुट क्रान्तिकारी विकल्प की अनुपस्थिति से आम जनता में जो निराशा है, उसके कारण वह सोचती है कि चलो, तबतक संसदीय वामपन्थी जो भी दो-चार आने की राहत दिला देते हैं, वही सही, क्योंकि क्रान्ति तो अभी काफ़ी दूर की बात है (या कि अब सम्भव नहीं है)। यानी आज भी संशोधनवाद जनता को अपने ऊपर पूँजीवाद को शासन करने की स्वीकृति देने के लिए तैयार करने का कार्य करता रहता है। इसे ही राजनीतिक वर्चस्व को स्वीकार करना कहते हैं।
ज्योति बसु इसी संशोधनवादी वाम राजनीति के एक महारथी थे। उनके जाने का दुख उनके संसदीय वामपन्थी साथी-सँघातियों को तो है ही, पूँजीवाद के कट्टर हिमायतियों, बुर्जुआ थिंक टैंकों और रणनीतिकारों को भी है और सुधारवादी मानस वाले मधयवर्गीय प्रगतिशीलों को भी। ज्योति बसु पुरानी पीढ़ी के संशोधनवादी थे। बुद्धदेव, सीताराम येचुरी, नीलोत्पल बसु और विजयन मार्का नये ज़माने वालों के मुकाबले वे ज्यादा खाँटी और पुराने फ्कम्युनिस्टी'' रंग ढंग वाले दिखते थे। पहले कभी गोपालन, सुन्दरैया, प्रमोद दासगुप्त, जैसों के मुक़ाबले ज्योति बसु ही फ्मॉडर्न'' माने जाते थे। मज़ाक में लोग उन्हें फ्पार्टी का उत्ताम कुमार'' भी कहते थे। ज्योति बसु संसदीय वामपन्थ की अधाोमुखी यात्राा के कई दौरों के साक्षी थे। तीन दशक पहले तक पार्टी में उन्हें सिद्धान्तकार और संगठनकर्ता का दर्जा, देश स्तर पर तो दूर, बंगाल स्तर पर भी हासिल नहीं था। बासवपुनैया, प्रमोद दासगुप्त, सुन्दरैया आदि की यह छवि थी। ज्योति बसु चुनावी राजनीति के स्टार थे, एक दक्ष राजनेता (स्टेट्समैन), कूटनीतिज्ञ (डिप्लोमैट) और प्रशासक थे। पंजाब के फ्जत्थेदार कॉमरेड'' हरकिशन सिंह सुरजीत घनघोर व्यवहारवादी (प्रैग्मेटिक) और जोड़तोड़ में माहिर-तिकड़मी राजनीतिज्ञ थे।
ज्योति बसु का जन्म 1914 में बंगाल के एक उच्च मधयवर्गीय कुलीन परिवार में हुआ था। 1935 में वे बैरिस्टरी की पढ़ाई करने लंदन गये। इस दौरान वे प्राय: लंदन स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स जाकर प्रख्यात सामाजिक जनवादी विद्वान हेराल्ड लास्की के भाषण सुनते थे। लास्की के विचारों ने ही उनके भीतर समाजवादी रुझान पैदा किया। 1937 में वे राष्ट्रवादी छात्राों के साथ 'इण्डिया लीग' और 'लंदन मजलिस' संस्थाओं में सक्रिय रहे। नेहरू, सुभाष और अन्य भारतीय नेताओं को लेबर पार्टी के नेताओं और समाजवादी नेताओं से मिलवाने का काम भी उन्होंने किया। इसी बीच 1939 में वे रजनी पाम दत्ता के सम्पर्क में आये, जो ब्रिटिश कम्युनिस्ट पार्टी के एक शीर्ष नेता थे। कम्युनिस्ट इण्टरनेशनल की भारत और उपनिवेश- विषयक नीतियों की व्याख्या करते हुए वे भारत और ब्रिटेन के पार्टी मुखपत्राों में लेख लिखा करते थे और प्राय: उनमें अपनी ओर से कुछ संशोधनवादी छौंक-बघार लगा दिया करते थे। वे एक अभिजात कम्युनिस्ट थे, जिनकी संशोधनवादी रुझानें उस समय भी थीं, जब ब्रिटेन की कम्युनिस्ट पार्टी का रंग अभी बदला नहीं था। बाद में संशोधनवाद की ओर पार्टी को धाकेलने में उनकी अग्रणी भूमिका रही थी। तो ऐसे व्यक्ति थे ज्योति बसु के राजनीतिक पथप्रदर्शक। दरअसल अपनी पीढ़ी के बहुतेरे उच्च मधयवर्गीय युवाओं की तरह ज्योति बसु भी एक रैडिकल राष्ट्रवादी थे जिन्हें समाजवाद के नारे आकृष्ट तो करते थे, लेकिन कम्युनिज्म की क्रान्तिकारी अन्तर्वस्तु को वे कभी भी आत्मसात नहीं कर पाये। चूँकि कम्युनिस्ट पार्टी भी उस समय अभी समाजवाद के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्रीय मुक्ति के लिए और जनवादी क्रान्ति के लिए लड़ रही थी, इसलिए बहुतेरे ऐसे रैडिकल जनवादी राष्ट्रवादी युवा उस समय पार्टी में शामिल हो रहे थे, जिन्हें कांग्रेस की समझौतापरस्ती की राजनीति रास नहीं आ रही थी। बहरहाल, युवा ज्योति बाबू में तब नौजवानी का जोश, वफुर्बानी का जज्बा और आदर्शवाद की भावना तो थी ही। स्वदेश-वापसी के बाद, वक़ालत करने के बजाय उन्होंने पेशेवर क्रान्तिकारी का जीवन चुना और मज़दूरों के बीच काम करने लगे। ग़ौरतलब है कि यह भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का वह दौर था जब पी.सी. जोशी के नेतृत्व में दक्षिणपन्थी भटकाव पार्टी पर हावी था। 1941 में ज्योति बसु ने बंगाल-असम रेलवे के मज़दूरों के बीच काम किया और उनके यूनियन सेक्रेटरी भी रहे। कुछ समय तक उन्होंने बंदरगाह और गोदी मज़दूरों के बीच भी काम किया।
कम्युनिस्ट पार्टी क़ानूनी घोषित की जाने के बाद 1943 में जब उसकी पहली कांग्रेस हुई तो उसमें ज्योति बसु प्रान्तीय संगठनकर्ता चुने गये। फ़िर चौथे राज्य सम्मेलन में उन्हें राज्य कमेटी में चुना गया। 1946 से देश एक ऐसे संक्रमण काल से गुज़रने लगा था, जिसमें प्रचुर क्रान्तिकारी सम्भावनाएँ निहित थीं। नौसेना विद्रोह, देशव्यापी मज़दूर हड़तालें, तेलंगाना-तेभागा-पुनप्रा वायलार के किसान संघर्ष ऌन ऐतिहासिक घटनाओं ने अगले तीन-चार वर्षों के दौरान पूरे देश को हिला रखा था। अपनी विचारधारात्मक कमज़ोरी, नेतृत्व में एकजुटता के अभाव और ढीले-ढाले सांगठनिक ढाँचे के कारण पार्टी इस निर्णायक घड़ी में पहल अपने हाथ में लेने में पूरी तरह विफ़ल रही (ऐसे अवसर वह पहले भी गँवा चुकी थी)। राष्ट्रीय आन्दोलन को नेतृत्व देने वाला बुर्जुआ वर्ग जनता की आकांक्षाओं के साथ विश्वासघात करते हुए साम्राज्यवादियों के साथ समझौते के साथ बुर्जुआ शासन की पूर्वपीठिका तैयार कर रहा था। बेशुमार साम्प्रदायिक ख़ून-ख़राबे के बाद देश का विभाजन हो रहा था। ऐसी राजनीतिक आज़ादी मिल रही थी जो अधाूरी और खण्डित थी। साम्राज्यवाद से निर्णायक विच्छेद के बजाय उसके आर्थिक हितों की सुरक्षा की गारण्टी दी जा रही थी। रैडिकल भूमि सुधार के मामले में भी कांग्रेस के विश्वासघात के संकेत मिल चुके थे। सार्विक मताधिकार के आधार पर चुने जाने के बजाय महज 12 फ़ीसदी आबादी द्वारा चुनी गयी संविधान सभा अत्यन्त सीमित जनवादी अधिकार देने वाला (और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें भी छीन लेने के इन्तज़ामों से लैस) वाग्जालों से भरा संविधान बना रही थी।
इस संक्रमण काल में कम्युनिस्ट पार्टी कन्फ़्रयूज़ थी, अनिर्णय का शिकार थी। रही-सही कसर रणदिवे की फ्वामपन्थी'' दुस्साहसवादी लाइन ने पूरी कर दी। नेहरू की भेजी हुई भारतीय पफौजों ने तेलंगाना किसान संघर्ष को कुचल दिया। लम्बी कमज़ोरियों और भूल-ग़लतियों के सिलसिले ने पार्टी को उसकी तार्किक परिणति तक पहुँचा दिया। तेलंगाना पराजय के बाद पार्टी पूरी तरह से संशोधनवादी हो गयी। चुनावी वामपन्थ का ज़माना आ गया। ज्योति बसु इस दौरान क्या कर रहे थे! किसान संघर्षों और जुझारू मज़दूर आन्दोलन को क्रान्तिकारी दिशा देने की किसी कोशिश के बजाय, पार्टी के निर्णय का पालन करते हुए उन्होंने 1946 की प्रान्तीय विधायिका का चुनाव लड़ा, रेलवे कांस्टीच्युएंसी से (सीमित मताधिकार के आधार पर), और विजयी रहे। उसी वर्ष भीषण साम्प्रदायिक दंगों के दौरान गाँधीजी जब बंगाल गये तो ज्योति बसु उनसे मिले और उनकी सलाह से एक शान्ति कमेटी बनायी और शान्ति मार्च निकाला। तेलंगाना किसान संघर्ष को लेकर पार्टी में जो कई लाइनों का संघर्ष था, उसमें उनकी कोई भूमिका नहीं थी। 1952 में जब पहले आम चुनाव हुए, तब वे बंगाल विधानसभा के सदस्य चुने गये और विधान चन्द्र राय की कांग्रेसी सरकार के शासनकाल के दौरान विपक्ष के नेता रहे। तबसे लेकर, सन् 2000 तक, 1972-77 की समयावधि को छोड़कर ज्योति बसु लगातार बंगाल की विधानसभा के लिए चुने जाते रहे। संसदीय राजनीति ही आधी शताब्दी तक उनका कार्यक्षेत्रा बनी रही। 1951 में वे पार्टी के बांग्ला मुखपत्रा 'स्वाधीनता' के सम्पादक-मण्डल के अधयक्ष चुने गये। 1953 में वे राज्य कमेटी के सचिव चुने गये। 1954 की मदुरै पार्टी कांग्रेस में वे केन्द्रीय कमेटी में और फ़िर पालघाट कांग्रेस में सेक्रेटेरियट में चुने गये। 1958 में अमृतसर की जिस विशेष कांग्रेस ने सोवियत पार्टी की बीसवीं कांग्रेस की ख्रुश्चेवी संशोधनवादी लाइन को सर्वसम्मति से स्वीकार किया था, उसी कांग्रेस में ज्योति बसु राष्ट्रीय परिषद में चुने गये थे। 1964 में जब भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का भाकपा और माकपा में विभाजन हुआ, तो यह संशोधनवाद और क्रान्तिकारी कम्युनिज्म के बीच का विभाजन नहीं था। वह विभाजन वस्तुत: संशोधनवाद और नवसंशोधनवाद के बीच था, नरमपन्थी संसदीय वामपन्थ और गरमपन्थी संसदीय वामपन्थ के बीच था, अर्थवाद और जुझारू अर्थवाद के बीच था। डांगे-राजेश्वर राव गुट (भाकपा) ख्रुश्चेवी संशोधनवाद का पूर्ण समर्थक था और नेहरूवादी फ्समाजवाद'' को प्रगतिशील राष्ट्रीय बुर्जुआ की नीति मानकर कांग्रेस का पुछल्ला बनने को तैयार था। विरोधी गुट (माकपा) ज्यादा शातिर संशोधनवादी था। माकपा नेतृत्व ख्रुश्चेवी संशोधनवाद की आलोचना करता था, लेकिन साथ ही चीन की पार्टी को भी अतिवाद का शिकार मानता था। सत्तारूढ़ सोवियत पार्टी को वह संशोधनवादी, लेकिन राज्य को समाजवादी मानता था। इस तर्क से कालान्तर में राज्य का समाजवादी चरित्रा भी समाप्त हो जाना चाहिए था, पर इसके उलट, माकपा ने कुछ ही वर्षों बाद सोवियत पार्टी को भी बिरादर पार्टी मानना शुरू कर दिया। माकपा नेतृत्व नेहरू सरकार को साम्राज्यवाद का जूनियर पार्टनर बन चुके इजारेदार पूँजीपति वर्ग का प्रतिनिधि मानकर उनके विरुद्ध राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा बनाकर संघर्ष करने की बात करता था।
माकपा का चरित्रा हालाँकि उसकी संसदीय राजनीति ने बाद में एकदम नंगा कर दिया, लेकिन 1964 में अपने गरम तेवर दिखाकर क्रान्तिकारी क़तारों के बड़े हिस्से को अपने साथ लेने में वह सफ़ल हो गयी। पार्टी संगठन के लेनिनवादी उसूलों के हिसाब से देखें तो माकपा का संशोधनवादी चरित्रा 1964 से ही एकदम साफ़ था। 1951 से जारी पार्टी के एकदम खुले, क़ानूनी, संसदीय चरित्रा और कार्यप्रणाली को माकपा ने यथावत् जारी रखा। पार्टी सदस्यता की प्रकृति रूस के मेंशेविकों से भी गयी-गुज़री थी। अमृतसर कांग्रेस में पार्टी संविधान में किये गये बदलाव को 1964 में यथावत् क़ायम रखा गया। पार्टी के लोक जनवादी क्रान्ति के कार्यक्रम के हिसाब से दीर्घकालिक लोकयुद्ध ही क्रान्ति का मार्ग हो सकता था, पर इसके उल्लेख से बचकर पार्टी कार्यक्रम में छलपूर्ण भाषा में फ्संसदीय और ग़ैर-संसदीय रास्ते'' का उल्लेख किया गया। कोई भी क्रान्तिकारी पार्टी बुर्जुआ संसदीय चुनावों का महज रणकौशल के रूप में इस्तेमाल करती है। संसदीय मार्ग को ग़ैर-संसदीय मार्ग के समकक्ष रखना अपने आप में संशोधनवाद है। 1967 में और 1969 में माकपा यही कहती थी कि वह संसद-विधानसभा का इस्तेमाल रणकौशल (टैक्टिक्स) के रूप में ही करती है। लेकिन 33 वर्षों तक बुर्जुआ व्यवस्था के अन्तर्गत बंगाल में शासन करते हुए (इनमें से 23 वर्षों तक ज्योति बसु के मुख्यमन्त्रिात्व में) उसने बुर्जुआ नीतियों को भरपूर वफ़ादारी के साथ लागू किया है और वर्ग संघर्ष की तैयारी के लिए चुनावों के टैक्टिकल इस्तेमाल के बजाय हर जनान्दोलन को कुचलने के लिए राज्यतन्त्र का बर्बर इस्तेमाल किया है। ज्योति बसु को इस साफ़गोई के लिए सराहा जाना चाहिए कि 1977 से 1990 के बीच दो-तीन बार उन्होंने कहा था कि 'हम पूँजीवाद के अन्दर एक राज्य में सरकार चला रहे हैं, समाजवाद नहीं ला रहे हैं।' माकपा पिछले दो-तीन दशकों से चुनाव के 'टैक्टिकल इस्तेमाल' वाला जुमला भूले से भी नहीं दुहराती। अब वह न केवल ख्रुश्चेवी शान्तिपूर्ण संक्रमण के सिद्धान्त को पूरी तरह से मौन स्वीकृति दे चुकी है और उसके और भाकपा के बीच व्यवहारत: कोई अन्तर नहीं रह गया है, बल्कि उसका आचरण एक निहायत भ्रष्ट एवं पतित सामाजिक जनवादी पार्टी जैसा ही है। भ्रष्टाचार का दीमक उसमें अन्दर तक पैठ चुका है (हालाँकि अन्य बुर्जुआ पार्टियों से फ़िर भी काफ़ी कम है) और बंगाल में राज्य मशीनरी के साथ माकपाई गुण्डाें-मस्तानों के समानान्तर तन्त्र की मौजूदगी ने सोशल फ़ासिस्ट दमन का माहौल बना रखा है।
जब माकपा-भाकपा का बँटवारा हो रहा था तो कुछ मधयमार्गी भी थे जो बीच में डोल रहे थे। फ़िर इनमें से कुछ भाकपा में गये कुछ माकपा में। जैसे, भूपेश गुप्त भाकपा में गये, ज्योति बसु माकपा में। ज्योति बसु शुरू से ही एक घुटे-घुटाये संसदीय वामपन्थी थे। 1967 में नक्सलबाड़ी किसान उभार के बाद एक नये धा्रुवीकरण की शुरुआत हुई। कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी कतारें भारी तादाद में माकपा से निकलकर नक्सलबाड़ी के झण्डे तले इकट्ठा होने लगीं। नक्सलबाड़ी पहले एक क्रान्तिकारी जनसंघर्ष के रूप में पूफटा लेकिन 1969 आते-आते उसपर चारु मजुमदार की फ्वामपन्थी'' आतंकवादी लाइन हावी हो गयी और फ़िर इसी लाइन पर भाकपा (मा.ले.) का निर्माण्ा हुआ। जो लोग आतंकवादी लाइन के विरोधी थे, वे भी राष्ट्रीय परिस्थितियों और कार्यक्रम की ग़लत समझ के कारण कोई क्रान्तिकारी विकल्प नहीं दे सके और यह पूरी धारा बिखराव का शिकार हो गयी। लेकिन 1967-68 में तो नक्सलबाड़ी उभार ने माकपा के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा कर दिया था।
1967 में बंगाल में संयुक्त मोर्चे की जो सरकार बनी थी, उसमें माकपा शामिल थी। ज्योति बसु उप-मुख्यमन्त्राी तथा वित्ता और परिवहन के मन्त्राी थे। माकपा ने सरकार से बाहर आकर नक्सलबाड़ी किसान उभार को समर्थन देने के बजाय, पहले तो वहाँ के स्थानीय पार्टी नेताओं एवं कतारों को समझाने-बुझाने का प्रयास किया। फ़िर सभी को पार्टी से बाहर किया गया और राज्य की सशस्त्रा पुलिस मशीनरी और (राज्य सरकार की अनुमति से) केन्द्रीय सशस्त्रा बलों का इस्तेमाल करके नक्सलबाड़ी आन्दोलन को बेरहमी से कुचल दिया गया। इसमें ज्योति बसु की उप-मुख्यमन्त्राी के रूप में अहम भूमिका थी। इस समय तक आन्दोलन पूरे देश में पफैल चुका था। हर राज्य में माकपा टूट रही थी। मा-ले पार्टी के गठन की प्रक्रिया शुरू हो रही थी। माकपा नेतृत्व ने सभी नक्सलबाड़ी समर्थकों को पार्टी से निकाल बाहर किया। 1969 में प. बंगाल में पुन: संयुक्त मोर्चे की जो सरकार बनी, उसमें भी ज्योति बसु उप-मुख्यमन्त्राी थे और साथ ही गृह, पुलिस और सामान्य प्रशासन विभाग भी उन्हीं के पास था। इस समय नक्सलबाड़ी तो कुचला जा चुका था, पर बंगाल के कई इलावफे धाधाक रहे थे। फ्वामपन्थी'' आतंकवादी कार्रवाइयाँ भी शुरू हो चुकी थीं। ज्योति बसु ने इस बार प्रतिरोधा को कुचलने के लिए पुलिस मशीनरी का बर्बर और बेधाड़क इस्तेमाल किया। 1972 के चुनावों में ज़बर्दस्त धाँधाली के बाद बंगाल में कांग्रेस की सरकार बनी। सिद्धार्थ शंकर रे मुख्यमन्त्राी बने। पूरे देश में तो आपातकाल जून 1975 में लगा, लेकिन बंगाल में नक्सलवादियों के दमन के नाम पर यन्त्राणा, फ़र्ज़ी मुठभेड़ों के ज़रिये फ़ासिस्ट पुलिस राज्य सिद्धार्थ शंकर रे ने 1972 में ही क़ायम कर दिया था। माकपा ने 1972 से 1977 तक विधानसभा का बहिष्कार किया। 1977 में आपातकाल हटने के बाद केन्द्र में जनता पार्टी शासन स्थापित हुआ और बंगाल में वाम मोर्चे का शासन क़ायम हुआ जो आज तक जारी है। ज्योति बसु मुख्यमन्त्राी बने और 2000 तक इस पद पर रहते हुए एक कीर्तिमान स्थापित किया। यह इतिहास का स्मरणीय तथ्य है कि सिद्धार्थ शंकर रे के शासनकाल के पहले, गृह एवं पुलिस मन्त्राालय सँभालते हुए नक्सलवाद के दमन के नाम पर पुलिस राज्य क़ायम करने का काम ज्योति बसु ने भी किया था।
1977 में ज्योति बसु ने जब बंगाल का मुख्यमंत्रिात्व सँभाला उस समय उनके सामने नक्सलबाड़ी की चुनौती नहीं थी। लेकिन नक्सलबाड़ी की एक नसीहत सामने थी, जिसपर सभी बुर्जुआ अर्थशास्त्राी, राजनीतिज्ञ और संशोधनवादी सहमत थे। सबकी कमोबेश एक ही राय थी और वह यह कि यदि नक्सलबाड़ी जैसे विस्पफोटों से और उसके फ्सम्भावित'' भयावह नतीजों से बचना है तो बुर्जुआ भूमि सुधारों की गति थोड़ी और तेज़ करनी होगी। ज्योति बसु ने इसी काम को 'आपरेशन बर्गा' के रूप में अंजाम दिया। आज माकपाई झाल-करताल लेकर 'ऑपरेशन बर्गा' का कीर्तन करते हैं। 'ऑपरेशन बर्गा' कोई क्रान्तिकारी भूमि सुधार नहीं था। वह ''ऊपर से किया गया,'' प्रशियाई टाइप, स्तॉलिपिन सुधार टाइप, मरियल बुर्जुआ भूमि सुधार कार्यक्रम था, जिसने आंशिक तौर पर भूमि के मालिकाने के सवाल को हल करके बंगाल की खेती में क्रमिक पूँजीवादी विकास की ज़मीन तैयार की और वहाँ कुलकों-पूँजीवादी किसानों के पैदा होने का आधार बनाया। ऐसे भूमि सुधार बहुतेरे अन्य प्रान्तों में हो चुके थे। बंगाल पीछे छूटा हुआ था। यदि रैडिकल चरित्रा की ही बात की जाये तो छठे दशक के शुरू में ही, अपने पहले शासनकाल के दौरान शेख़ अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर में ज्यादा रैडिकल बुर्जुआ भूमि-सुधार कार्यक्रम लागू किया था।
1977 तक भारत का पूँजीवाद काफ़ी मज़बूत हो चुका था और कृषि के पूँजीवादीकरण की प्रक्रिया को तेज़ करके, रहे-सहे र्अद्ध-सामन्ती अवशेषों को समाप्त करके एक व्यापक राष्ट्रीय बाज़ार का निर्माण करना उसकी ज़रूरत थी। ज्योति बसु ने 'ऑपरेशन बर्गा' के द्वारा पूँजीवादी भूमि-सुधार के इसी कार्यक्रम को कुशलतापूर्वक लागू किया और भारतीय पूँजीवाद की ऐतिहासिक सेवा की। 'ऑपरेशन बर्गा' ने काश्तकार किसानों को आंशिक मालिकाना हक़ देकर पूँजीवादी खेती के विकास के साथ ही इन नये छोटे-बड़े मालिक किसानों में माकपा का नया सामाजिक आधार और वोट बैंक तैयार किया। गाँवों में जो बड़े मालिक किसानों का ताक़तवर हिस्सा पैदा हुआ, उसे राजनीतिक सत्ता में (आर्थिक ताक़त के अनुरूप) भागीदारी भी चाहिए थी। यह उसे एक ओर माकपा पार्टी तन्त्र के स्थानीय मनसबदार के रूप में हासिल हुआ (बंगाल में माकपा की पार्टी मशीनरी प्रशासन मशीनरी के साथ मिलकर काम करती है) और दूसरी ओर पंचायती राज ने उसे लूटने-खाने और शासन करने का मौक़ा दिया। पूँजीवादी पंचायती राज का 'ट्रेण्ड-सेटर' प्रयोग वास्तव में ज्योति बसु ने किया था जिसे राजीव गाँधी शासन काल के दौरान कांग्रेस ने अपना लिया था (हालाँकि उतने प्रभावी ढंग वह इसे लागू नहीं कर पायी)।
बंगाल के गाँवों में पूँजीवादी विकास का सिलसिला जब कुछ और आगे बढ़ा तो जो छोटे मालिक किसान पूँजीवादी शोषण का शिकार हो रहे थे, उनका धीरे-धीरे माकपा व वाम मोर्चा से मोहभंग होने लगा। माकपा के स्थानीय कार्यकर्ताओं (जो प्राय: नवधानिक कुलक या ग्रामीण मधयवर्ग के लोग थे) की गुण्डागर्दी और भ्रष्टाचार ने इसमें विशेष भूमिका निभायी। उधार नवधानिक कुलकों का एक हिस्सा भी लूट के माल और स्थानीय सत्ता के बँटवारे के बढ़ते अन्तरविरोधों के चलते माकपा से दूर हटा। गाँवों में इन्हीं के बीच तृणमूल कांग्रेस ने (और कहीं-कहीं कांग्रेस ने भी) अपना नया वोट बैंक तैयार किया है।
वर्ष 1977 में ज्योति बसु के नेतृत्व में वाम मोर्चा सरकार की विभिन्न सुधारवादी कार्रवाइयों ने नगरों-महानगरों में मधय वर्ग को विशेष तौर पर अपनी ओर खींचा। संगठित मज़दूरों को भी शुरू में कुछ आर्थिक लाभ मिले। सबसे बड़ी बात यह थी सिद्धार्थ शंकर रे के काले आतंक राज को भूलने और कांग्रेस को माफ़ करने के लिए मधयवर्ग और मज़दूर कत्ताई तैयार नहीं थे। यही कारण था कि जब ज्योति बसु सरकार के बुर्जुआ सुधारों का 'स्कोप' समाप्त हो गया, शासन-प्रशासन में बढ़ता भ्रष्टाचार साफ़ दीखने लगा और माकपा के स्थानीय नेताओं की दादागिरी भी बढ़ने लगी, तब भी बंगाल की जनता विशेषकर शहरी मधय वर्ग और औद्योगिक मज़दूर उसे मजबूरी का विकल्प मानते रहे। बंगाल के शहरों में जनवादी चेतना अधिक रही है और सिद्धार्थ शंकर रे के शासनकाल को याद करके बंगाल की जनता सोचती रही कि जनवादी अधिकारों के नज़रिये से माकपा शासन को बनाये रखना उसकी विवशता है।
इस बीच ज्योति बसु, माकपा और वाम मोर्चे का सामाजिक जनवादी चरित्रा ज्यादा से ज्यादा नंगा होता चला गया। भद्रपुरुष ज्योति बाबू बार-बार मज़दूरों को हड़तालों से दूर रहने और उत्पादन बढ़ाने की राय देने लगे, जबकि मज़दूरों की हालत लगातार बद से बदतर होती जा रही थी। ज्योति बसु विदेशी पूँजी को आमन्त्रिात करने के लिए बार-बार पश्चिमी देशों की यात्राा पर निकलने लगे (कभी छुट्टियाँ बिताने तो कभी आर्थिक-तकनीकी मदद के लिए 1990 तक रूस और पूर्वी यूरोप तो जाते ही रहते थे)। देशी पूँजीपतियों को पूँजी-निवेश के लिए पलक-पाँवड़े बिछाकर आमन्त्रिात किया जाने लगा। देश के तमाम बड़े पूँजीपति (विदेशी कम्पनियाँ भी) पूँजी निवेश के लिए बंगाल के परिवेश को अनुकूल बताने लगे। दिक्वफत अब उन्हें हड़तालों से नहीं थी, बल्कि माकपा के उन ट्रेड यूनियन क्षत्रापों से थी जो मज़दूरों से वसूली करने के साथ ही मालिकों से भी कभी-कभी कुछ ज्यादा दबाव बनाकर वसूली करने लगते थे।
जब 1991 से नरसिंह राव की सरकार ने उदारीकरण-निजीकरण की नीतियों की शुरुआत की तो माकपा देश स्तर पर तो उसका विरोध कर रही थी, लेकिन बंगाल में ज्योति बसु की सरकार उन्हीं नीतियों को लागू कर रही थी। चीन का फ्बाज़ार समाजवाद'' माकपा को नवउदारवादी लहर में बहने का तर्क दे रहा था, दूसरी ओर उदारीकरण-लहर को कुछ ''मानवीय चेहरा'' देने मात्रा की सिफ़ारिश करते हुए माकपा 'सेफ़्टी वॉल्व' का और पैबन्दसाज़ी का अपना पुराना सामाजिक जनवादी दायित्व भी निभा रही थी। गत् शताब्दी के अन्तिम दशक के उत्तारर्ाद्ध तक माकपा की नीतियों से मज़दूर वर्ग और शहरी निम्न मधयवर्ग को अब आंशिक सुधार की भी उम्मीद नहीं रह गयी थी। पूँजी निवेश से रोज़गार पैदा होने की उम्मीदें मिट्टी में मिल चुकी थीं। कलकत्ता के औद्योगिक मज़दूरों की स्थिति अन्य औद्योगिक केन्द्रों से भी बदतर थी।
माकपा ने मुहल्ले-मुहल्ले तक, मज़दूर बस्तियों से लेकर दुर्गापूजा समितियों तक अपने मस्तान नुमा कार्यकर्ताओं का ऐसा नेटवर्क तैयार कर लिया था कि अस्पताल में भरती होने से लेकर स्कूल में एडमिशन तक का काम उनके बिना नहीं हो सकता था। माकपा प्रभुत्व वाली मज़दूर यूनियनों और छात्रा यूनियनों के प्रभाव क्षेत्रा में राजनीतिक पैठ की किसी कोशिश को गुण्डागर्दी से दबा दिया जाता था। इसी प्रकार का माफ़िया तन्त्र गाँवों में पार्टी दफ़्रतरों और पंचायती राज संस्थाओं के इर्द-गिर्द निर्मित हो चुका था। यह सब कुछ ज्योति बसु के ही शासनकाल के दौरान हुआ था। इसके बावजूद विशेषकर पिछले दो या तीन चुनावों में वाममोर्चा यदि जीता तो उसका मुख्य कारण था सी.पी.एम. के पार्टी माफ़िया तन्त्र का आतंककारी, प्रभावी नेटवर्क और किसी कारगर बुर्जुआ चुनावी विकल्प का अभाव। तृणमूल ने एक हद तक स्वयं वैसा ही नेटवर्क खड़ा करके (लोहे को लोहे से काटने की नीति अपनाकर), गाँवों में मालिक किसानों के प्रतिर्स्पद्धी गुटों और माकपा से निराश ग़रीब किसानों को साथ लेकर तथा कांग्रेस के साथ मोर्चा बनाकर जब प्रभावी चुनौती पेश की है तो प्रबुद्ध शहरी मधयवर्ग का बड़ा हिस्सा भी इधार आकृष्ट हुआ है। सिंगूर और नन्दीग्राम ने माकपा की मिट्टी और अधिक पलीद करने का काम किया है। चुनावी राजनीति के दायरे में पहली बार माकपा के सितारे गर्दिश में नज़र आ रहे हैं। इस दायरे के बाहर क्रान्तिकारी विकल्प की तलाश करते हुए मेहनतकश ग्रामीण आबादी का सबसे तबाह हिस्सा और रैडिकल शहरी युवाओं का एक हिस्सा ''वामपन्थी'' दुस्साहसवादी राजनीति की ओर मुड़ा है। तीसरी ओर, औद्योगिक मज़दूरों और रैडिकल छात्रों-युवाओं का एक हिस्सा क्रान्तिकारी जन राजनीति की नयी दिशा और नये रूपों के सन्धान की ओर उन्मुख हुआ है। बंगाल की राजनीति आज एक मोड़ पर खड़ी है। आगे बदला हुआ परिदृश्य चाहे जैसा भी हो, इतना तय है कि माकपा के ''सुनहरे दिन'' अब बीत चुके हैं।
सच पूछें, तो इस पराभव की शुरुआत तो ज्योति बसु के शासन काल के दौरान ही हो चुकी थी। यूँ तो स्वास्थ्य कारणों से 2000 में उन्होंने मुख्यमन्त्राी पद छोड़ा था, लेकिन इज्ज़त बचाकर निकल लेने के लिए, ससम्मान मंच से विदा होने के लिए, उन्होंने बिल्कुल सही समय का चुनाव किया था। व्यक्तिगत तौर पर एक कसक रह गयी थी 1996 में वी.पी. सिंह द्वारा प्रस्ताव रखने के बावजूद माकपा ने उन्हें देश का प्रधानमन्त्री बनने से रोक दिया था। इसके पहले 1989 में भी अरुण नेहरू और चन्द्रशेखर ने वी.पी. सिंह की जगह उन्हें प्रधानमन्त्री बनने का प्रस्ताव रखा था, पर तब वे खुद ही नहीं चाहते थे। 1996 में उनका कैल्कुलेशन यह था कि यदि वे प्रधानमन्त्री बन जायेंगे तो अन्य बुर्जुआ पार्टियाँ बहुत दिनों तक तो सरकार चलने नहीं देंगी। इस तरह मरने से पहले प्रधानमन्त्री बनने की उनकी निजी साधा भी पूरी हो जायेगी और सत्ताच्युत होने के बाद यह कहकर ''शहीद'' बनने का मौक़ा मिल जायेगा कि जनहित की नीतियाँ लागू करते ही साम्राज्यवादियों-पूँजीपतियों और बुर्जुआ पार्टियों ने उनकी सरकार गिरा दी। पार्टी में प्रकाश करात के हावी गुट का कैल्कुलेशन यह था कि केन्द्र स्तर पर यदि दो-ढाई वर्षों तक भी सरकार चलती रही तो नवउदारवादी नीतियों को लागू करने के चलते माकपा की लँगोटी उतर जायेगी और बची-खुची इज्ज़़त भी नीलाम हो जायेगी। अब इनमें से कौन ज्यादा सही सोच रहा था, यह अटकल लगाना हमारा काम नहीं है। जो भी हो, पूँजीवादी संसदीय जनवाद की इतनी सेवा करने के बावजूद ज्योति बसु को यदि प्रधानमन्त्री बनने की साधा लिये-लिये इस दुनिया से जाना पड़ा, यदि अपने ही ''कामरेडों'' ने किये-दिये पर पानी फ़ेर दिया, तो वे कर भी क्या सकते थे! ज्यादा से ज्यादा भड़ास निकाल सकते थे और 1996 के पार्टी के निर्णय को ''ऐतिहासिक भूल'' बताकर उन्होंने यही किया था।
ज्योति बसु प्रधानमन्त्री भले ही नहीं बन सके, उन्हें उनके अवदानों के लिए न केवल अपने संसदीय वामपन्थी साथियों से, बल्कि बुर्जुआ नेताओं, विचारकों और बुद्धजिीवियों से तथा बुर्जुआ मीडिया से भरपूर सम्मान मिला। उनके निधन पर सभी ने शोकविह्नल होकर उन्हें याद किया। क्रान्तिकारी उथल-पुथल के तूफ़ानों से डरने वाले, भलेमानस मधयवर्ग के बहुतेरे शान्तिवादी, पैबन्दवादी, करुणामय हृदय वाले बुद्धिजीवियों ने भी पुरानी पीढ़ी के इस संसदीय वामपन्थी महारथी को भावुक होकर श्रद्धांजलि दी।